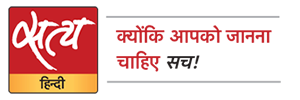क्या भारत नस्लकुशी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है? या यह इस सरकार के विरोधियों द्वारा किया जा रहा भय का प्रचार है, अतिरंजित आशंका है? सरकार ही नहीं, भारत को बदनाम करने का षड्यन्त्र है? नस्लकुशी या जनसंहार शब्द का प्रयोग जिम्मेदारी और सावधानी से किया जाना चाहिए, छिटपुट हिंसा की घटनाओं के उदाहरण से बात को बढ़ा-चढ़ाकर उस हिंसा को जनसंहार की पूर्वपीठिका बतलाना कितना उचित है? और नस्लकुशी तो किसकी?
पिछले एक महीने से यह चर्चा चारों तरफ होने लगी है। राजनीतिशास्त्री और विशेषज्ञ जो भारतीय नहीं हैं, यह चेतावनी देने लगे हैं कि अगर विश्व समुदाय ने भारत सरकार को पाबंद नहीं किया तो इसके पूरे आसार हैं कि नस्लकुशी शुरू हो जाए।
सबसे ताज़ा चेतावनी ‘जेनोसाइड वाच’ के अध्यक्ष ग्रेगोरी स्टेनटन ने दी है। यह संस्था इसपर नजर रखती है कि दुनिया में कहाँ-कहाँ नस्लकुशी की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं और वह उनके बारे में उस देश, समुदाय और विश्व समुदाय को सावधान करती रहती है।
स्टेनटन ने कहा कि उन्होंने रवांडा में जनसंहार या नस्लकुशी की भविष्यवाणी की थी और वह दुर्भाग्य से सच निकली। वे भारत में भी जनसंहार के लक्षण देख रहे हैं।
स्टेनटन नस्लकुशी के अध्येताओं में अग्रणी हैं और उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है । विशेषज्ञों और विद्वानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए । लेकिन भारत में विशेषज्ञ सरकार के आदेश को दुहराते हैं और उसके प्रवक्ता बन गए हैं । और जो सरकारी विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें भारत विरोधी या सरकार विरोधी कहकर इस कदर बदनाम कर दिया गया है कि हमारे यहाँ विशेषज्ञता मज़ाक बन गई है।
हाल के कोविड संक्रमण के प्रसंग में सरकारी विशेषज्ञों और सरकार से बाहर के और भारत के बाहर के विशेषज्ञों के संक्रमण के आकलन में इतना बड़ा अंतर था और है कि सामान्य लोगों के लिए तय करना कठिन है कि कौन सच बोल रहा है। फिर वह यह भी कैसे जाने कि उसके साथ हो क्या रहा है? क्या ये दो विरोधी विशेषज्ञ एक ही ज्ञान के क्षेत्र के हैं, क्या इनका मतांतर ईमानदार है या इसके कारण राजनीतिक हैं? क्या मुझे अपना विशेषज्ञ उसकी राजनीति देखकर चुनना चाहिए? अगर ऐसा हुआ, यानी अगर राजनीतिक पसंद विशेषज्ञता के स्वीकार की शर्त बन गई तो ज्ञान की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी और वह किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है।
वह वैसे ही है जैसे आप समंदर में जहाज पर हों और दिशासूचक यंत्र आपकी मर्जी से दिशा बतलाने लगेगा और आप खतरे में पड़ जाएंगे।
धर्म संसदों का आयोजन
स्टेनटन को सुना जाना चाहिए। हाल में हरिद्वार, दिल्ली, रायपुर और अन्य स्थलों पर हुई धर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों और ईसाइयों के संहार का उकसावा देनेवाले भाषण दिए गए। भाषण देनेवाले कोई साधारण लोग नहीं थे। वे विभिन्न अखाड़ों और धार्मिक संप्रदायों के मुखिया थे। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के नेता उनके चरण छूते देखे गए हैं। उनके अनुयायियों की संख्या हजारों-लाखों में है।
आस्थावान उनके प्रवचन श्रद्धा से सुनते हैं और उन्हें आदेश मानते हैं। यानी उनकी बात का व्यापक महत्त्व है। अगर वे यह कहें कि मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा हैं, कि हिंदुओं के बचे रहने के लिए मुसलमानों का सफाया कर देना चाहिए, कि उन्हें अपने घर में हथियार जमा करने चाहिए तो क्या उनके श्रोता इसे मजाक मानकर हवा में उड़ा देंगे? या अगर उनमें से एक छोटे हिस्से ने भी इसे गंभीरता से लिया तो इसके परिणाम क्या होंगे?
धर्म संसदों के इस आयोजन को इसके साथ मिलाकर देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगामी चुनाव को 80% और 20% के बीच का युद्ध बता चुके हैं। 80 कौन और 20 कौन, इसकी व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं है।
प्रधानमंत्री अपनी कूटभाषा में ‘कपड़ों से पहचानो’, ‘श्मशान-कब्रिस्तान’, आदि के जरिए दो आबादियाँ किस तरह अलग हैं और क्यों एक छोटी आबादी बड़ी जनसंख्या के लिए खतरा है, बार-बार बतलाते रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने हाल मे तेलंगाना में अपने भाषण में बाबर, निजाम और ओवैसी का नामोनिशान मिटा देने का वादा किया।
यह भी जनसंहार का ही उकसावा है, भले ही वह धर्म संसद की तरह एकदम सीधी ज़ुबान में न किया गया हो। लेकिन दोनों तरह के उकसावों का अर्थ एक दूसरे के साथ ही खुलता है।
असम के मुख्यमंत्री ने असम जाकर फिर यह कहा है कि 35% आबादी बाकी 65% के लिए समस्या खड़ी कर रही है और अगर असम के लोग एकजुट नहीं हुए तो अगले 20 साल में असम के स्कूलों में अरबी भाषा में पढ़ाई की जाएगी। यह साफ़ तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पैदा करने की कोशिश है।
जिन्होंने नस्लकुशी का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि वह कोई एक विस्फोट नहीं है। वह भूकंप या ऐसी प्राकृतिक आपदा की तरह नहीं है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वह एक धीरे धीरे विकसित होनेवाली प्रक्रिया है और उसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं।
पहले आबादियों को हर मामले में अलग किया जाता है। यह स्थापित किया जाता है कि दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं। एक का बने रहना दूसरे के लिए हर तरह से नुकसानदेह है, बल्कि उसके अस्तित्व मात्र के लिए वह खतरा है। फिर इस विरोधी समूह की निशानदेही की जाती है। वर्गीकरण हमेशा से नस्लकुशी का पहला निर्णायक कदम होता है। यह कानून के द्वारा औपचारिक बना दिया जाता है।
विरोधी समूह पैदा करके उससे घृणा या ईर्ष्या के कारण पैदा किए जाते हैं। जर्मनी में यहूदी समृद्ध थे और समाज के हर दायरे में अग्रणी थे। शेष जर्मन समुदाय में उनसे ईर्ष्या उत्पन्न करना कठिन नहीं था। यौन असुरक्षा पैदा करना एक दूसरा कदम है। यह जर्मनी में भी किया गया था। भारत में मुसलमानों के प्रति यौन ईर्ष्या कोई 100 साल से पैदा की जा रही है। वे मांसाहारी होने के कारण अधिक वीर्यवान हैं, हिंदू लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, जाने कितने दशकों से चलाए जा रहे इस प्रचार ने मुसलमान पुरुषों की छवि षड्यंत्रकारी शत्रु की बना दी है।
चूँकि वे हिंदू औरतों को बहका लेते हैं, उनके इस कृत्य का बदला मुसलमान औरतों पर कब्जा करके लिया जाना चाहिए। हाल के सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुसलमान औरतों की ऑनलाइन नीलामी इसी ईर्ष्या का एक अश्लील नमूना थी।
संख्याभय पैदा करना जनसंहार की तैयारी के लिए अनिवार्य है। हिंदुओं में यह डर लगातार बैठाया जा रहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या उनसे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों की संख्या को नियंत्रित करना ज़रूरी है। यह कानून से और दूसरे साधनों से किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे यह अपने आपको बचाने के लिए ज़रूरी लगने लगता है।
रवांडा का उदाहरण
नस्लकुशी को लेकर सामाजिक सहमति बनाना, उसका स्वागत करने को लोगों को तैयार करने में वक्त लगता है लेकिन वह सहमति बना ली जा सकती है। रवांडा इसका ताज़ा उदाहरण है। लेकिन उसके साथ म्याँमार में रोहिंग्या मुसलमानों के संहार में समाज की भागीदारी, उसके पहले श्रीलंका में तमिल हिंदुओं के संहार के लिए सिंहली बौद्ध समाज की हिंसक सहमति को भी याद रखना चाहिए।
संहार के लिए चिह्नित समूह की सांस्कृतिक पहचान को भी साझा जगहों से मिटा देना, यानी सांस्कृतिक संहार शारीरिक संहार की पूर्वशर्त है।
उसे यह अहसास दिलाना कि राष्ट्र की पहचान गढ़ने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसे पहले से हीन स्थिति में गिरा देने के लिए और खुद को किनारे किए जाने की नियति मान लेने के लिए ज़रूरी है। फैजाबाद, इलाहाबाद, मुग़लसराय स्टेशन का नाम बदलना, दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम बदल देना इसी सांस्कृतिक संहार का हिस्सा है।
बहुसंख्यक समाज में चिह्नित समुदाय को अपराधी की तरह पेश करना, उसे कीड़ा, दीमक, आतंकवादी कहकर बुलाना, यह बतलाना कि उसकी वजह से समाज का पानी गंदा हो रहा है, वह गंदगी है, उसे निकालकर फेंक देना स्वच्छता की रक्षा के लिए ज़रूरी है। यह सब कुछ एक तैयारी है।
क्या सारी आबादी एक बार में खत्म किया जाना नस्लकुशी है? इसकी परिभाषा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, यह है कि अगर चिह्नित समूह के एक हिस्से को भी खत्म किया जाता है तो भी वह नस्लकुशी है क्योंकि उसके पीछे इरादा पूरे समुदाय को खत्म करने का है। संख्या महत्वपूर्ण है लेकिन हिंसा के पीछे का विचार अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए गुजरात और मुजफ्फरनगर की हिंसा भी उसी दायरे में रखी जाएगी।
भारत में यह और आसान है। आज़ादी के बाद से ही हिंसा का धारावाहिक चल रहा है। जबलपुर, भिवंडी, बिहारशरीफ, भागलपुर, नेल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, मुज़फ्फरनगर की हिंसा को इस दायरे में रखा जा सकता है।
इस तरह एक समुदाय के प्रति हिंसा को लोग सामान्य मानने लगते हैं। कल तक जिस गाँव में मुसलमान थे, अजान होती थी, आज वह उस आवाज़ से खाली है लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। मुसलमानों की रोजी रोटी छीनकर उसे दे दिए जाने का वादा आकर्षक है।
यह सबकुछ मिलकर नस्लकुशी की ज़मीन तैयार करते हैं और उसे सह्य ही नहीं, आवश्यक मानने को बड़ी आबादी को तैयार कर देते हैं।
अगर हम जनसंहार के खुलेआम नारों और भाषणों को स्वीकार्य मानते हैं तो जनसंहार को स्वीकार करना भी हमारे लिए कठिन न होगा। लेकिन यह अवश्यम्भावी नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर इसे रोका जा सकता है। यह तब हो सकता है जब जनसंहार की राजनीति को चुनाव में पराजित किया जाए और न्याय प्रक्रिया के सहारे जनसंहार का उकसावा देनेवालों को दंडित करने के लिए दबाव बनाए रखा जाए।
इसे नियति मान लेना कि यह होगा ही और कुछ न करना जनसंहार को दावत देना है ।समाज को बार-बार बताने की ज़रूरत है कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है और इसे रोकना ही सबसे बड़ी राजनीति है।